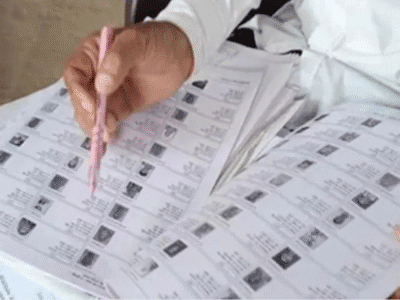~हरीश तिवारी
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ‘राजनीति’ शब्द कभी त्याग, तपस्या और राष्ट्र-निर्माण का पर्याय हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में यह विमर्श का विषय बन गया है कि क्या राजनीति अपने मूल पथ से भटक गई है? क्या वह जनसेवा का माध्यम न रहकर व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता की भूख और शोषण का एक परिष्कृत औज़ार बनती जा रही है? यह प्रश्न केवल बौद्धिक चर्चा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस आम आदमी की पीड़ा है जो हर पाँच साल में एक नई उम्मीद के साथ मतदान केंद्र तक जाता है, पर अंततः खुद को छला हुआ महसूस करता है।
गौरवशाली अतीत बनाम वर्तमान की कड़वाहट
एक समय था जब ‘नेता’ शब्द का अर्थ था—समाज का मार्गदर्शक और अन्याय के विरुद्ध एक निर्भीक आवाज़। गांधी, शास्त्री और जेपी जैसे व्यक्तित्वों ने राजनीति को ‘सेवा के धर्म’ के रूप में स्थापित किया था। उस दौर में नेता की पहचान उनके सादे जीवन और उच्च विचारों से होती थी।
आज स्थिति इसके ठीक उलट प्रतीत होती है। वर्तमान में नेता की परिभाषा अक्सर सत्ता-समीकरण, बाहुबल, धनबल और अवसरवाद के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई है। जनता के सेवक अब ‘जनता के स्वामी’ की मुद्रा में दिखाई देते हैं।
सेवा बनाम सत्ता: उद्देश्य का विस्थापन
पहले राजनीति एक ‘मिशन’ थी, आज वह कई मायनों में एक ‘प्रोफेशन’ और ‘सत्ता का सौदा’ बन गई है।
- दूरी का बढ़ना: जनप्रतिनिधि पहले गलियों में दिखते थे, आज वे ऊंचे मंचों, बुलेटप्रूफ गाड़ियों और सोशल मीडिया के फिल्टरों के पीछे छिप गए हैं।
- चुनावी चक्र: चुनाव के समय लुभावने वादे और जीत के बाद उन वादों को फाइलों में दबा देना—यह एक ऐसा चक्र बन गया है जिसने राजनीति की साख (Credibility) को सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई है।
नेता की असली कसौटी: भाषण नहीं, आचरण
एक वास्तविक जननायक की पहचान पोस्टर, होर्डिंग्स या सोशल मीडिया पर मिलने वाले ‘लाइक्स’ से नहीं हो सकती। नेता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। - संकट का साथी: जो बाढ़ की विभीषिका में जनता के साथ खड़ा हो, जो महामारी के दौर में अस्पताल की चौखट पर संघर्ष करे और जो अन्याय के विरुद्ध सत्ता की परवाह किए बिना आवाज उठाए, वही सच्चा नेता है।
- संवेदना की राजनीति: राजनीति आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आँसुओं को पोंछने की कला होनी चाहिए। जो नेता फाइलों के आंकड़ों से ज्यादा जनता के अभावों से जुड़ा होता है, वही जन-मन पर राज करता है।
राजनीति का नैतिक संकट
आज की राजनीति एक गहरे नैतिक संकट से गुजर रही है। इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं: - धनबल और बाहुबल: टिकट वितरण से लेकर चुनाव जीतने तक, धन की भूमिका ने ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं।
- पहचान की राजनीति: विकास के मुद्दों को दरकिनार कर जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर ध्रुवीकरण करना एक आसान चुनावी रणनीति बन गई है।
- दिखावे की संस्कृति: सोशल मीडिया के इस युग में ‘काम’ से ज्यादा ‘काम के प्रचार’ पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे धरातल की हकीकत ओझल होती जा रही है।
समाधान: सुधार की दिशा
राजनीति को पुनः ‘सेवा के पथ’ पर लौटाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है: - चरित्र आधारित राजनीति: पारदर्शिता और जवाबदेही को केवल कानूनी नहीं, बल्कि अनिवार्य नैतिक मानक बनाया जाए। ‘राइट टू रिकॉल’ जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
- मूल्यों से लैस युवा: राजनीति में युवाओं का स्वागत केवल उनकी उम्र के कारण नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद नए विजन, संवेदना और साहस के कारण होना चाहिए।
- सतत संवाद: केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे पाँच साल ‘जनसुनवाई’ की एक जवाबदेह व्यवस्था होनी चाहिए।
जनता की सामूहिक जिम्मेदारी
लोकतंत्र में जनता केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक है। यदि राजनीति प्रदूषित हुई है, तो उसे स्वच्छ करने का दायित्व भी नागरिकों पर है। - सजग मतदान: हमें जाति, धर्म या तात्कालिक लालच के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और नियत को देखकर वोट देना होगा।
- निरंतर निगरानी: लोकतंत्र पाँच साल में एक बार वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन सरकार से सवाल पूछने और उसे जवाबदेह बनाए रखने का नाम है।
राजनीति स्वयं में न तो गंदी है और न ही शोषण का माध्यम। यह वह पवित्र धारा है जो राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करती है। इसे स्वार्थ के कीचड़ से निकालकर सेवा की गंगा बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यदि हम चाहते हैं कि राजनीति शोषण का औज़ार न बने, तो हमें ऐसे नेतृत्व को गढ़ना होगा जो सत्ता के गलियारों से ज्यादा जनता की गलियों में नजर आए।