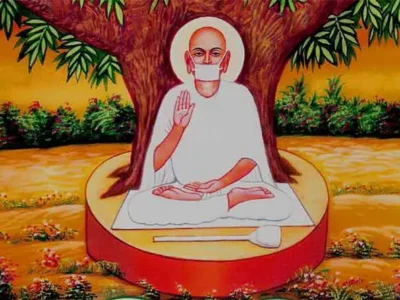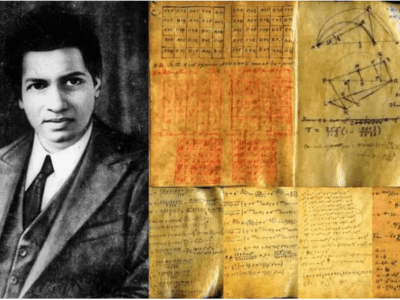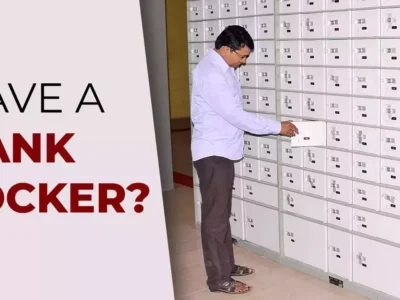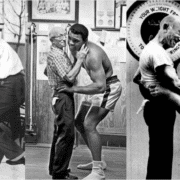Declaration of War: युद्ध, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में तनाव और अनिश्चितता पैदा करता है। जब दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू होता है, तो यह न केवल सैनिकों, बल्कि आम नागरिकों और वैश्विक समुदाय को भी प्रभावित करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव ने एक बार फिर युद्ध की घोषणा (Declaration of War) को चर्चा में ला दिया है। यह प्रक्रिया क्या है, और भारत ने अपने इतिहास में इसे कैसे अपनाया? यह लेख भारत युद्ध इतिहास (India War History) की इस जटिल प्रक्रिया को सरल और आकर्षक तरीके से नई पीढ़ी के लिए समझाता है, जो समाचारों और इतिहास में रुचि रखती है।
जब कोई देश दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है, तो यह एक औपचारिक और गंभीर कदम होता है। यह कदम राजनैतिक, कानूनी और सैन्य परिणामों के साथ आता है। आमतौर पर, युद्ध की घोषणा देश की सरकार या शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है। इसमें युद्ध के कारण, लक्ष्य और विरोधी देश का स्पष्ट उल्लेख होता है। यह घोषणा संसद, राष्ट्रपति या समकक्ष प्राधिकरण के माध्यम से हो सकती है। भारत में, हालांकि, अधिकांश युद्धों में औपचारिक घोषणा के बजाय त्वरित सैन्य कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है। यह प्रक्रिया नई पीढ़ी को यह समझने में मदद करती है कि युद्ध जैसी स्थिति में सरकारें कैसे काम करती हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच तीन प्रमुख युद्ध—1947-48, 1965 और 1971—हो चुके हैं। इनमें से केवल 1971 के युद्ध में संसद की औपचारिक मंजूरी ली गई थी। 1947-48 के कश्मीर युद्ध में, जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बिना संसद की मंजूरी के सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। यह युद्ध भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय में लड़ा गया, जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा था। नई पीढ़ी, जो इतिहास और समसामयिक घटनाओं में रुचि रखती है, इस घटना से यह सीख सकती है कि आपातकाल में त्वरित निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
1962 का भारत-चीन युद्ध एक और उदाहरण है, जहां कोई औपचारिक युद्ध की घोषणा (Declaration of War) नहीं हुई। चीन ने अचानक हमला किया, और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। युद्ध के दौरान संसद में चर्चा हुई, लेकिन मंजूरी बाद में दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को एकजुट होने का आह्वान किया। यह युद्ध भारत के लिए एक सबक था, जिसने सैन्य तैयारियों और रणनीति को मजबूत करने की जरूरत को उजागर किया। नई पीढ़ी के लिए यह समझना जरूरी है कि युद्ध केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक होता है।
1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी बिना औपचारिक घोषणा के शुरू हुआ। पाकिस्तान ने “ऑपरेशन जिब्राल्टर” के तहत छिपकर हमला किया, और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। संसद ने 3 सितंबर 1965 को एक प्रस्ताव पारित किया, जो युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि सरकार को समर्थन देने वाला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को पूरी छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने इस युद्ध में मजबूत स्थिति हासिल की। यह घटना नई पीढ़ी को यह दिखाती है कि नेतृत्व का साहस और रणनीतिक फैसले युद्ध के परिणाम को कैसे बदल सकते हैं।
1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र पर हमला किया। इसके जवाब में, 4 दिसंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। यह भारत के इतिहास में भारत युद्ध इतिहास (India War History) का एकमात्र ऐसा उदाहरण है, जहां संसद ने औपचारिक रूप से युद्ध को मंजूरी दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दिया। यह कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, जो यह सीख सकती है कि दृढ़ संकल्प और एकता कितनी शक्तिशाली हो सकती है।
1999 का कारगिल युद्ध एक और महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था, लेकिन इसे युद्ध के बजाय “ऑपरेशन विजय” नाम दिया गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की, और संसद ने एकमत से पाकिस्तान की निंदा की। हालांकि, कोई औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को निर्देश दिए, और भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। यह घटना नई पीढ़ी को यह समझाती है कि आधुनिक युद्धों में औपचारिक घोषणाओं की बजाय त्वरित और रणनीतिक कार्रवाइयां अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
भारत में युद्ध की घोषणा की कोई स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति, जो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, सरकार की सलाह पर फैसले लेते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की स्थिति में संसद की मंजूरी की बात करता है, लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति (CCS) इस तरह के फैसले लेती है। यह जानकारी नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, जो यह समझना चाहती है कि सरकारें संकट के समय कैसे काम करती हैं।
आधुनिक समय में, युद्ध की औपचारिक घोषणा कम ही देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष को रूस “विशेष सैन्य अभियान” कहता है, जबकि दुनिया इसे युद्ध मानती है। युद्ध के दौरान जिनेवा संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन अपेक्षित होता है, जो युद्धबंदियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह कहानी न केवल युद्ध की घोषणा (Declaration of War) की प्रक्रिया को समझाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत ने अपने इतिहास में विभिन्न युद्धों को कैसे लड़ा और जीता।
#DeclarationOfWar, #IndiaWarHistory, #IndiaPakistanWar, #MilitaryHistory, #IndianPolitics
ये भी पढ़ें: Gang Rape of Woman in Titwala: टिटवाला में 21 वर्षीय युवती के साथ 5 पुरुषों ने किया सामूहिक बलात्कार, 7 के खिलाफ केस