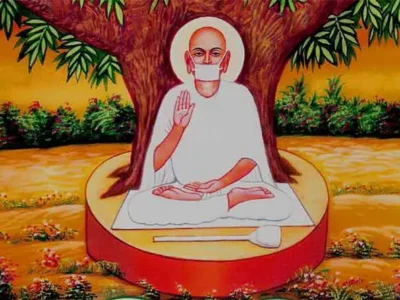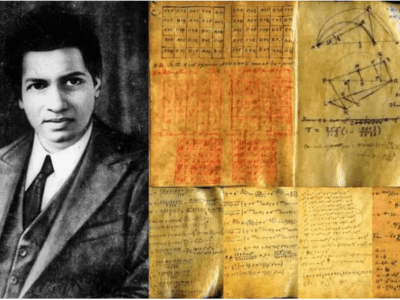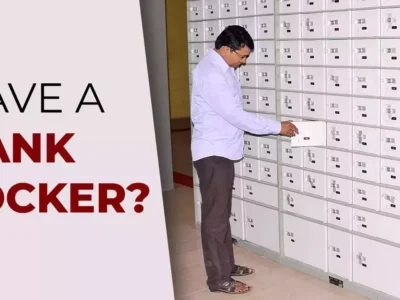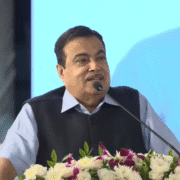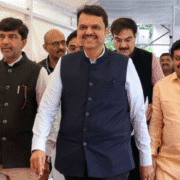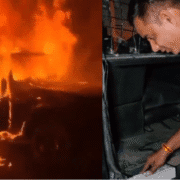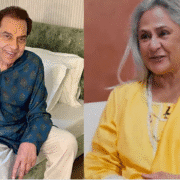Right to Die: ‘राइट टू डाई’ यानी गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अब भारत में कानूनी रूप से लागू होने वाला एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इसे कानूनी मान्यता दी है। लेकिन यह इच्छा मृत्यु या Euthanasia नहीं है, बल्कि इसे Passive Euthanasia के रूप में जाना जाता है। इस नए कानून के तहत, गंभीर रूप से बीमार या लाइलाज रोग से जूझ रहे मरीज यह तय कर सकते हैं कि वे अपनी जीवनरक्षक चिकित्सा को जारी रखना चाहते हैं या नहीं।
Right to Die: कर्नाटक ने क्यों लागू किया ‘राइट टू डाई’?
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू डाई विद डिग्निटी’ यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी थी। इसके तहत Passive Euthanasia और Living Will को सशर्त वैध करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति जो जीवन के अंतिम चरण में है, वह अपनी चिकित्सा को रोकने का फैसला कर सकता है ताकि वह बिना अनावश्यक कष्ट के प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर सके।
कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए यह कानून लागू किया है। इसके तहत मरीजों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी जीवनरक्षक दवाओं, वेंटिलेटर, कृत्रिम जीवन-समर्थन प्रणाली को बंद करने का निर्णय खुद ले सकें।
‘राइट टू डाई’ और इच्छा मृत्यु में क्या अंतर है?
‘राइट टू डाई विद डिग्निटी’ यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार और इच्छा मृत्यु (Euthanasia) को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
- राइट टू डाई विद डिग्निटी में मरीज को यह तय करने का अधिकार होता है कि वह अपने जीवनरक्षक इलाज को जारी रखना चाहता है या नहीं। मरीज अपनी ‘लिविंग विल’ के जरिए पहले से यह तय कर सकता है कि अगर वह किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसे कृत्रिम जीवनरक्षक उपकरणों पर न रखा जाए।
- इच्छा मृत्यु (Euthanasia) में डॉक्टर या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से जानबूझकर किसी मरीज की जीवनलीला समाप्त की जाती है, ताकि उसकी पीड़ा खत्म हो सके। यह या तो इंजेक्शन के जरिए (Active Euthanasia) किया जाता है या फिर इलाज रोककर (Passive Euthanasia)।
- Passive Euthanasia का मतलब किसी मरीज को जीवनरक्षक दवाएं, वेंटिलेटर या अन्य कृत्रिम चिकित्सा सहायता देना बंद कर देना है, ताकि वह स्वाभाविक रूप से अपनी अंतिम सांस ले सके। जबकि Active Euthanasia यानी इच्छा मृत्यु में मरीज को कृत्रिम रूप से मौत देने का कार्य किया जाता है, जिसे भारत में अवैध माना गया है।
कैसे काम करता है यह कानून?
कर्नाटक में अब कोई भी व्यक्ति अपनी लिविंग विल (Living Will) बना सकता है, जिसमें वह पहले से ही लिखकर यह निर्देश दे सकता है कि अगर वह किसी लाइलाज बीमारी या कोमा की स्थिति में चला जाए, तो उसे कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली पर न रखा जाए।
अब अस्पतालों और डॉक्टरों को इस फैसले का सम्मान करना होगा, बशर्ते कि प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तय दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
भारत में अन्य राज्यों ने इसे क्यों लागू नहीं किया?
कर्नाटक के अलावा अभी तक भारत के किसी अन्य राज्य ने इसे लागू नहीं किया है। इसके पीछे कई कारण हैं:
- कानूनी जटिलताएं: सुप्रीम कोर्ट ने इसे सशर्त कानूनी मान्यता दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है, जिससे अन्य राज्यों को इसे लागू करने में कठिनाई हो रही है।
- धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण: भारत जैसे देश में मृत्यु से जुड़े विषय संवेदनशील माने जाते हैं। कई धर्मों में इसे आत्महत्या के समान माना जाता है, इसलिए लोग इसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते।
- राजनीतिक अनिश्चितता: राजनीतिक दल इस विषय पर खुलकर चर्चा करने से बचते हैं, क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकता है।
- चिकित्सा समुदाय की चिंताएं: डॉक्टरों को डर रहता है कि अगर लिविंग विल के फैसले में कोई गलती हो गई, तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कर्नाटक ने ऐसा क्यों किया?
कर्नाटक भारत के उन राज्यों में से एक है, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां के अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को लेकर जागरूकता अधिक है।
इसके अलावा, कर्नाटक का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत है और यहां लिविंग विल और पैसिव युथनेशिया को लागू करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं।
क्या अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे?
अब जब कर्नाटक ने यह कानून लागू कर दिया है, तो संभावना है कि अन्य राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।
महाराष्ट्र, गोवा और केरल जैसे राज्य इस पर विचार कर रहे हैं, और अगर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति या कानून बनाती है, तो यह पूरे देश में लागू हो सकता है।
क्या भारत में इच्छा मृत्यु (Active Euthanasia) कानूनी है?
नहीं, भारत में Active Euthanasia यानी इच्छा मृत्यु अवैध है और इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ Passive Euthanasia और Living Will को सशर्त कानूनी मान्यता दी है, जिसका मतलब है कि मरीज सिर्फ अपने इलाज को रोकने का फैसला कर सकता है, लेकिन किसी और को उसे मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
‘राइट टू डाई’ का भविष्य क्या है?
कर्नाटक का यह कदम भारतीय कानून और चिकित्सा नीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह मरीजों को अत्यधिक पीड़ा से बचाने और गरिमा के साथ मरने का अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालांकि, इसे पूरे देश में लागू करने के लिए अभी कई कानूनी, सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को पार करना होगा। लेकिन अगर अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति बनाती है, तो यह भारत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित हो सकता है।
#RightToDie, #Euthanasia, #LivingWill, #PassiveEuthanasia, #SupremeCourt
ये भी पढ़ें: Middle Class in India: भारत में मिडिल क्लास कौन हैं और कितने लोग इसमें आते हैं?